स्वयं ही स्वयं के मार्ग में, अंतिम ज्ञान जो होता है, उसमें साधक का आत्मा ही ब्रह्म होता है। लेकिन, ऐसे साक्षात्कार से पूर्व, अपने पिण्ड स्वरुप में, साधक जो बूँद सरिका होता है, वो स्वयं को सागर रूप में ही देखता है। इसलिए, यहाँ पर आत्मा और ब्रह्म, और बूंद और सागर के एकापन की बात होगी, जिसमे आत्मा ही ब्रह्म है, और बूँद ही सागर है।
ये अध्याय भी आत्मपथ, ब्रह्मपथ या ब्रह्मत्व पथ श्रृंखला का अंग है, जो पूर्व के अध्याय से चली आ रही है।
ये भाग मैं अपनी गुरु परंपरा, जो इस पूरे ब्रह्मकल्प (Brahma Kalpa) में, आम्नाय सिद्धांत से ही सम्बंधित रही है, उसके सहित, वेद चतुष्टय से जो भी जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी लोक में हो, उस सब को और उन सब को समरपित करता हूं।
और ये भाग मैं उन चतुर्मुखा पितामह ब्रह्म को ही स्मरण करके बोल रहा हूं, जो मेरे और हर योगी के परमगुरु योगेश्वर कहलाते हैं, जो, योगिराज, योगऋषि, योगसम्राट, योगगुरु और महेश्वर भी कहलाते हैं, जो योग और योग तंत्र भी होते हैं, जिनको वेदों में प्रजापति कहा गया है, जिनकी जिनकी अभिव्यक्ति हिरण्यगर्भ ब्रह्म और कार्य ब्रह्म भी कहलाती है, जो योगी के ब्रह्मरंध्र विज्ञानमय कोश में उनके अपने पिंडात्मक स्वरूप में बसे होते हैं और ऐसी दशा में वो उकार भी कहलाते हैं, जो योगी की काया के भीतर अपने हिरण्यगर्भात्मक लिंग चतुष्टय स्वरूप में होते हैं, जो योगी के ब्रह्मरंध्र के भीतर जो तीन छोटे छोटे चक्र होते हैं उनमें से मध्य के बत्तीस दल कमल में उनके अपने ही हिरण्यगर्भात्मक सगुण आत्मा स्वरूप में होते हैं, जो जीव जगत के रचैता, ब्रह्मा कहलाते हैं, और जिनको महाब्रह्म भी कहा गया है, जिनको जानके योगी ब्रह्मत्व को पाता है, और जिनको जानने का मार्ग, देवत्व और जीवत्व से होता हुआ, बुद्धत्व से भी होकर जाता है।
ये अध्याय, “स्वयं ही स्वयं में” के वाक्य की श्रंखला का ये दसवां अध्याय है, इसलिए, जिसने इससे पूर्व के अध्याय नहीं जाने हैं, वो उनको जानके ही इस अध्याय में आए, नहीं तो इसका कोई लाभ नहीं होगा।
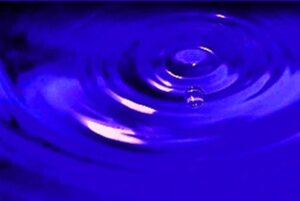
बूंद और सागर, … आत्मा और ब्रह्म …
“स्वयं ही स्वयं में” जाकर भी, तुम उसको तबतक नहीं जान पाओगे, जबतक तुम, तुम्हारी अपनी भीतर की अवस्था में, तुम्हारी चेतना में, उसके जैसा नहीं हो जाओगे।
जैसे जबतक बूंद अपनी चेतना में ही सागर नहीं हो जाती है, तबतक वो बूंद सागर में रह कर भी, सागर को ना ही जान पाती है और ना ही उस सागर में विलीन ही हो पाती है।
वैसे ही तुम भी हो, जो उस सागर रूपी ब्रह्म में अनादि कालों से बसे होने के बाद भी, उसको जान नहीं पाए हो।
जबतक तुम तुम्हारी अपनी भीतर की अवस्था में, वो ब्रह्म ही नहीं हो जाओगे, तबतक तुम उस ब्रह्म में बसे होने के बाद भी और वो ब्रह्म तुम्हारे अपने आत्मस्वरूप में होने के बाद भी, तुम उसे जान नहीं पाओगे।
इसलिए, यदि उसको जानना है, तो तुम्हें तुम्हारी अपनी भीतर की अवस्था में, वो ही होना पड़ेगा, नहीं तो तुम भी वो ही बोलोगे, जो आज के कुछ मनीषि बोलते हैं, कि उसे कौन जान पाया है।
जो साधक उसकी अपनी भीतर की अवस्था में, उस ब्रह्म के जैसा नहीं होता, वो साधक उस ब्रह्म को ना तो जान पाता है और ना ही उस ब्रह्म में विलीन हो पाता है।
और जो साधक उसकी अपनी भीतर की अवस्था में, उस ब्रह्म के जैसे ही हो जाता है, वो साधक ही उस ब्रह्म को जान पाता है, और वो भी उस साधक के अपने आत्मस्वरूप में।
लेकिन ऐसा जानने के बाद भी, वो साधक उस ब्रह्म को अपनी वाणी में पूर्णरूपेण बतला ही नहीं पायेगा, क्योंकि वो ब्रह्म शब्दातीत और वाणीतीत ही होता है।
ब्रह्म का ज्ञाता ब्रह्म ही है, … ब्रह्म का ज्ञाता ही ब्रह्म है … ब्रह्म ही ब्रह्म का ज्ञाता है …
इसलिए, कुछ ब्रह्मदृष्टा वेद मनीषी ऐसे ही बोल गए थे, कि…
ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म ही होता है।
ब्रह्म हुए बिना, ब्रह्म को नहीं जाना जाता।
इसलिए, यदि तुमको ब्रह्म को जानना है, तो अपनी भीतर की अवस्था में, तुम्हें ब्रह्म ही होना पड़ेगा…, क्योंकि उसको जानने का कोई और मार्ग है ही नहीं।
और यही कारण है, कि यदि ब्रह्म को जानना है, तो साधक को ब्रह्म भावापन होना ही पड़ेगा।
और यही संकेत, ब्रह्मसूत्र के प्रथम सूत्र में, भगवान वेदव्यास ने अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के सूत्र में भी दिया है।
और यही संकेत कुछ सिद्ध गण भी दे गए हैं, जैसे कि…
ब्रह्म को केवल ब्रह्म ही जानता है। जो ब्रह्म नही, वो ब्रह्म का ज्ञाता भी नहीं।
ब्रह्म का ज्ञाता, ब्रह्म ही होता है। ब्रह्म का ज्ञाता ही ब्रह्म होता है।
ब्रह्म हुए बिना, ब्रह्म को नहीं जाना जाता, इसलिए यदि ब्रह्म को जानना है, तो ब्रह्म ही हो जाओ।
वैसे भी, तुम्हारी वास्तविकता में, तुम्हारे आत्मस्वरूप में…,तुम वो ब्रह्म ही तो हो।
अब आगे बढ़ता हूं…
बूँद सागर में, और सागर बूंद में बसा होता है … आत्मा ही ब्रह्म …, बूंद ही सागर …
तुम उसमें अनादि कालों से बसे हुए हो, और वो भी तुममें, अनादि काल से बसा हुआ है। लेकिन तब भी, तुम उसे इसीलिए नहीं जान पाये हो, क्यूंकि तुम्हारी अपनी भावनात्मक चेतना में, तुम वो ब्रह्म नहीं हो पाए हो।
इसलिए, जिस समय से, तुम अपने भीतर की दशा में, अपनी ही चेतना में, वो ब्रह्म हो जाओगे, उसी समय से तुम तुम्हारी अपनी वास्तविकता में, तुम्हारे अपने ही आत्मास्वरूप में, उस ब्रह्म को ही पाओगे।
जैसे बूंद सागर में विलीन होके, सागर ही हो जाती है, वैसे ही तुम्हारा और प्रजापति ब्रह्म का नाता भी है।
जैसे जबतक बूंद उसकी अपनी चेतना में ही सागर नहीं हो जाती है, तबतक वो सागर में पड़ी होने के बाद भी, स्वयं को सागर नहीं मानती। वैसे ही तुम भी हो।
तुम भी उसी ब्रह्म रूपी सागर में पड़े हो, और वो ब्रह्म तुम्हारे भीतर तुम्हारे आत्मस्वरूप में भी है, लेकिन तब भी तुम अपने वास्तविक स्वरूप को, अपने ब्रह्मस्वरूप को नहीं जानते हो। और तुम्हारी ऐसी अज्ञानमय अवस्था भी तब है, जब तुम तुम्हारी अपनी वास्तविकता में, तुम्हारे अपने ही आत्मस्वरूप में, वो ब्रह्म ही हो।
जैसे बूंद के मूल, उत्कर्ष मार्ग और गंतव्य, तीनो में, वो सागर ही होता है, वैसे ही तुम भी हो, जिसके मूल, उत्कर्ष मार्ग और गंतव्य, तीनो में, तुम्हारी वास्तविकता में, तुम वो ब्रह्म ही हो।
जबतक तुम भी तुम्हारी अपनी ही चेतना में, उसी प्रजापति में विलीन होके, तुम्हारे अपने भीतर की अवस्था में, वो प्रजापति ही नहीं हो जाओगे, तबतक तुम ना तो उस प्रजापति को अपने आत्मस्वरूप मे पाओगे, ना ही उस प्रजापति के किसी प्रधान स्वरुप को जान ही पाओगे।
और जबतक ऐसा नहीं होगा, तबतक तुम कुछ भी कर लो, कोई भी उपाधि धारण कर लो, किसी भी लोक में महिमा मंडित हो जाओ, देवता ही क्यों न हो जाओ, उस ब्रह्म को जान नहीं पाओगे।
बूँद स्वयं को सगर कब मानती है …
सागर में पड़ी हुई बूंद भी, अपने को सागर तब ही मानती है, जब वो स्वयं ही, उसकी अपनी चेतना में, सागर हो जाती है।
जबतक वो बूंद ऐसी नहीं होती, तबतक चाहे वो बूंद सागर में ही बसी हुई क्यों न हो, वो सागर नहीं हो पाएगी।
तुम भी ऐसी बूंद के समान ही हो, क्योंकि वो प्रजापति ब्रह्म ही तुम्हारे भीतर तुम्हारे आत्मस्वरूप में हैं। और इसके साथ साथ, तुम भी उस प्रजापति ब्रह्म के ही अनंत स्वरूप के भीतर बसे हुए हो।
वो ब्रह्म तुम में है, और तुम भी उसी ब्रह्म में बसे हुए हो, और ये दशा भी वैसी है, जैसे सागर में पड़ी हुई बूंद के भीतर भी तो वही सागर ही होता हैं।
जैसे वो बूंद सागर में होती है और वो सागर ही बूंद के मूल में होता है, और अंततः वोही सागर, बूँद के गंतव्य में भी पाया जाता है, वैसा ही तुम्हारा और उस प्रजापति ब्रह्म का नाता भी है।
जैसे बूंद उसी सागर से उदय हुई थी, उसी सागर से चली थी, वैसे ही तुम भी हो, जो उसी प्रजापति ब्रह्म से चले थे, उसी प्रजापति ब्रह्म से पृथक होके, अलग होके, अपने ही बूंद स्वरूप में जीव हुए थे।
जैसे अपने ही जीवन में वो बूंद, कभी भाप, कभी बादल, कभी झरना, कभी नाला, कभी नदी और कभी तो पृथ्वी के भीतर ही होती है, वैसे ही तुम भी हो, कभी भूचर जीव, कभी जलचर जीव और कभी नभचर जीव और कभी तो किसी और जीव के पेट में।
जैसे वो बूंद सागर से उदय होके, बारम्बार किसी न किसी स्वरूप में आती रहती है, वैसे ही तुम भी हो, जो उसी प्रजापति से उदय हुए थे, और इसके बाद बारम्बार किसी न किसी रूप में, जन्म और मरण के फेर में पड़े हुए हो।
बूँद, नदी और सागर … देवलोक और ब्रह्मलोक की गति …
जैसे जब बूंद, किसी पहाड़ के झरने से, नदी में गिरती है, तो वो हर्ष उल्हास से नाचती हुई, उस नदी में जाती है…, वैसे ही तुम भी हो, जब तुम किसी नदी रूपी देवलोक में चले जाते हो, तो वहां भी नाचते गाते, ऊधम मचाते हुए जाते हो।
देवलोकों की ओर गति में, हर्ष उल्लास होता ही है। और ये हर्ष उल्लास बिलकुल वैसा ही होता है, जैसे झरने की बूँदें, नदी में गिरती हैं । और ऐसे समय पर, उस झरने की सारी बूंदे, उछलती कूदती, नाचती जाती, ऊधम मचाती, कलकल करती हुई ही, किसी पहाड़ के झरने से नदी में गिरती हैं।
लेकिन, जैसे ही वो बूंद, जो पूर्व में, एक तेज धारा वाली नदी में होती है, और अपने उस नदी की धारा रुपी उत्कर्ष मार्ग पर चलते चलते, सागर के समीप आ जाती है, तब वो बहुत चौड़ी होके, कई भागो में बंटके, शांत हो जाती है…, वैसे ही तुम भी होगे, जब तुम ब्रह्मपथ पर जाके, बस ब्रह्मलीन हो ही रहे होगे।
उस समय जब तुम ब्रह्मलीन होने को होगे, तब तुममें कोई भी हर्ष उल्हास, उछलना कूदना, नाचना गाना, ऊधम मचाना नहीं होगा।
तुम्हारी उस अन्त गति में, तुम बस शांत चित्त होके ही ब्रह्मलीन होगे, बिल्कुल वैसे ही, जैसे वो नदी अपनी अंत गति में, शांत होके ही सागर में विलीन होने को जाति है। इसलिए, जबतक तुम अपने भीतर से ही शांत नहीं होगे, तबतक तुम ब्रह्मलीन भी नहीं हो सकते।
ब्रह्म की इस रचना के समस्त इतिहास में, कोइ दौड़ता भागता, उछलता कूदता, नाचता गाता, ऊधम मचाता, महिमा मंडित होता साधक, कभी भी ब्रह्म को नहीं पाया है।
ब्रह्माण्ड के इतिहास में, जिस भी साधक ने ब्रह्म को पाया है, तो वो साधक उसी नदी के समान शांत चित्त और अपनी चेतना में चौड़ा होता है, जिस समय पर वो नदी सागर में विलीन हो रही होती है।
जैसे जब नदी सागर में विलीन होती है, तब वो बहुत चौड़ी होती है, और वैसे ही साधक की विशालकाए चेतना स्तिथी होती है, जब वो साधक ब्रह्मलीन हो रहा होता है।
जैसे जब नदी सागर में विलीन होती है, तो वो कई भागों में भी बंट जाती है …, वैसे ही किसी साधक की प्रकृत स्थिति होती है, जब वो ब्रह्मलीन हो रहा होता है।
ब्रह्मलीन होते समय साधक की प्रकृति स्थिति …
तो अब मैं साधक की इस प्रकृति स्थिति को कुछ सांकेतिक रूपों में ही बतलाता हूँ, जब वो ब्रह्मलीन हो रहा होता है।
साधक के ब्रह्मलीन होने से पूर्व, जो कुछ भी इस ब्रह्माण्ड का है, और वो साधक की काया के भीतर पड़ा हुआ है, वो सबकुछ अपने अपने कारणों में स्वयं ही विलीन होता चला जाता है। इसलिए, ब्रह्मलीन अवस्था से पूर्व, वो साधक भी उसी सागर में विलीन होती हुई नदी के समान, बंटा हुआ सा प्रतीत होता हैं।
जबतक जो कुछ भी इस ब्रह्माण्ड का है, अर्थात जो ब्रह्माण्ड की दशाएं तुम्हारे भीतर हैं, उन सबको, उनके ही ब्रह्माण्डीय अवस्थाओं में लौटाओगे नहीं, तबतक ब्रह्माण्ड से अतीत होके, ब्रह्मलीन कैसे होगे।
जैसे अपना व्यर्थ का भार त्याग के ही पक्षी ऊँची उड़ान भर सकता है, वैसे ही तुम्हारी वो अंतिम उड़ान भी होगी, जब तुम भी अपने गंतव्य की उड़ान भरने लगोगे, और बस ब्रह्मलीन हो ही रहे होगे।
क्यूंकि ब्रह्म वो पूर्ण सन्यासी है, इसलिए ब्रह्मलीन होते समय, तुम्हारी अपनी मानसिक स्थिति में, तुमको भी उस ब्रह्म के समान, पूर्ण सन्यासी ही होना पड़ेगा। जो साधक ब्रह्म के समान पूर्ण सन्यासी नहीं है, वो ब्रह्मलीन कैसे होगा?…, थोड़ा सोचो तो।
लेकिन उस पूर्ण सन्यास का मार्ग भी तो पूर्ण त्याग को ही लेके जाता है, जिसका मार्ग साधक के भीतर के ब्रह्माण्ड को, उस बहार के ब्रह्माण्ड में ही लौटा देता है, जिसमें साधक अपने काया स्वरुप में बसा हुआ होता है।
इसलिए, ब्रह्मलीन होने का मार्ग, सर्वत्र के त्याग से ही होकर जाता है…, क्यूंकि इसका कोई और मार्ग है भी तो नहीं।
अब आगे बढ़ता हूँ …
और यही कारण है, कि ब्रह्मलीन होने की प्रक्रिया में, साधक की काया के भीतर, कई सारे सिद्ध शरीर, स्वयं ही प्रकट होते चले जाते हैं ।
और इस प्रक्रिया में, जैसे जैसे समय बीतता है, वैसे वैसे ये सभी सिद्ध शरीर जो साधक की काया के भीतर बसे हुए ब्रह्माण्ड की पृथक पृथक अवस्थाओं को दर्शाते हैं, वो अपने अपने कारणों में, स्वयं ही विलीन होते चले जाते है।
इस ब्रह्मलीन या ब्रह्म में विलीन होने की प्रक्रिया में, जो उस साधक के उत्कर्ष मार्ग की अंतिम उड़ान होती है, जैसे जैसे समय बीतता है, वैसे वैसे साधक के भीतर बहुत सारे सिद्ध शरीर स्वयं प्रकट होते ही चले जाते हैं, और ये सिद्ध शरीर, साधक के भीतर बसे हुए ब्रह्माण्ड की प्रमुख अवस्थाओं को दर्शाते हैं।
इस उत्कर्ष मार्ग की अंतिम प्रक्रिया में, ये सभी ब्रह्माण्डीय अवस्थाएँ साधक के सिद्ध शरीरों के रूप में ही स्वयंप्रकट होती हैं, और इसके बाद वो सिद्ध शरीर, उनके अपने अपने ब्रह्माण्डीय कारणों में विलीन भी होते ही चले जाते हैं।
और इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात, साधक के भीतर का ब्रह्माण्ड, जो वही ब्रह्माण्ड है जिसमें वो साधक बसा भी हुआ है, उसमें विलीन हो जाता है…, और अंततः वो साधक, ब्रह्माण्ड से ही अतीत हो जाता है।
जबतक तुम तुम्हारे भीतर के ब्रह्माण्ड और उसकी ब्रह्माण्डीय अवस्थाओं को, उनके अपने मूल कारणों में ही लौटाओगे नहीं, तबतक तुम ब्रह्माण्ड से अपना नाता तोडोगे कैसे?…, थोड़ा सोचो तो ।
और जबतक तुम ब्रह्माण्ड से अपना नाता तोडोगे नहीं, तबतक तुम इस जीव जगत से अतीत कैसे होंगे?…, इस बिंदु पर भी थोड़ा सोचो तो।
और जबतक तुम इस जीव जगत से ही अतीत नहीं होगे, तबतक तुम मुक्त कैसे होंगे…, इसपर भी थोड़ा सोचो तो?।
जबतक तुम अपने भीतर बसी हुई समस्त ब्रह्माण्डीय अवस्थाओं का भार, अपने ऊपर से उतार नहीं दोगे, तबतब तुम इस ब्रह्माण्ड से ऊपर कैसे उड़ोगे, अर्थात अतीत कैसे होंगे…, थोड़ा इसपर भी सोचो तो? I
जबतक तुम ब्रह्माण्ड से अतीत नहीं होंगे, तबतक तुम्हारी उत्कर्ष की उड़ान उस गंतव्य रुपी, पूर्ण सन्यासी, अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म को कैसी जाएगी, जो ब्रह्माण्ड के भीतर और ब्रह्माण्ड के स्वरुप, दोनों में बसा हुआ भी…, लेकिन तब भी वो वास्तव में ब्रह्माडातीत ही है I
जीव जगत से अतीत की अवस्था को ही तो मुक्ति कहते हैं।
जैसे जबतक कोई वायुयान अपने अतिरिक्त भार को उतार कर हल्का नहीं होता, तबतक तो वो लंबी और ऊंची उड़ान भी नहीं भर पाता…, वैसे ही साधक के उत्कर्ष की उड़ान भी होती है।
इसलिए, जबतक साधक उसका अपना अतिरिक्त भार, जो उसके भीतर बसे हुए ब्रह्माण्ड का होता है, उसको त्यागता नहीं है, तबतक वो साधक भी उसके उत्कर्ष मार्ग की अंतिम उड़ान, जिसमें वो साधक ब्रह्मलीन होता है…, वो भर नहीं पाता।
जबतक जो कुछ भी इस ब्रह्माण्ड का है, उसे लौटाओगे नहीं, तबतक तुम हलके भी नहीं हो पाओगे। और जबतक ऐसे हलके नहीं होगे, तबतक तुम भी अपने उत्कर्ष मार्ग की अंतिम उड़ान, जो ब्रह्मलीन अवस्था को लेके जाती है …, वो भर नहीं पाओगे।
एक बात याद रखो, कि तुम्हारी अपकर्ष या उत्कर्ष की गति के परिपेक्ष्य में, या तो तुम जीव जगत के हो सकते हो, या इस जीव जगत से परे, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म के।
लेकिन उत्कर्ष मार्ग की उस अंतिम उड़ान के परिपेक्ष में, अर्थात कैवल्य मार्ग में, तुम इस जीव जगत से परे, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म के ही होंगे क्यूंकि उत्कर्ष मार्ग के अमूल गंतव्य में, वो निराधार, निरालम्बा, निर्विकल्प निर्गुण निराकार ही होता है…, और वो भी तुम्हारे अपने ही वास्तविक स्वरुप, अर्थात तुम्हारे अपने ही आत्मस्वरुप में I
यदि जीव जगत के होके रहोगे, तो तुम्हे कुछ भी त्यागने की आवश्यकता नहीं I
और यदि तुम उस सर्वव्याप्त, सार्वभौम, सर्वसाक्षी, गंतव्य रूपी निर्गुण निराकार के होने के इच्छुक हो, तो तुम्हें समस्त जीव जगत को ही त्यागना पड़ेगा, जिसके भीतर तुम अपने जीव रूप में बसे हुए हो, और जो उसके अपने सूक्ष्म संस्कारिक प्राथमिक ब्रह्माण्ड स्वरूप में, तुम्हारे भीतर ही बसा हुआ हैI
और यही कारण है, की उत्कर्ष मार्ग में, अंतिम गति का पथ भी त्याग का ही होता है, और इसी प्रक्रिया में वो साधक उसके अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहम् से ही समस्त जीव जगत का त्याग कर देता है।
उस अंतिम उड़ान का जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार, साधक के आत्मस्वरूप में ही करवाती है…, त्याग के अतिरिक्त कोई और मार्ग है ही नहीं।
और उस अंतिम उड़ान से पूर्व, वो त्याग भी समस्त जीव जगत का ही होता है, नाकि किसी एक या दो ब्रह्माण्डीय या जीव अवस्थाओं का।
जबतक ब्रह्माण्ड को ही त्यागोगे नहीं, ब्रह्माण्ड से अतीत कैसे होगे। और वो ब्रह्माण्ड जिसको तुम्हें तुम्हारे अपने उत्कर्ष मार्ग की अंतिम गति में त्यागना है, वो भी तो तुम्हारी काया के भीतर ही बसा हुआ है I
कभी कोई अपने से बाहर की अवस्था को भी त्याग सकता है?, …, इसपर भी थोड़ा सोचो तो I इसलिए त्याग की प्रक्रिया भी साधक के भीतर से ही चलित होकर, साधक के भीतर बसे हुए जीव जगत का ही होता है I
जबतक ब्रह्माण्ड से ही अतीत नहीं होगे, तो कैवल्य मुक्ता कैसे होगे…, मोक्ष को कैसे प्राप्त होगे?…, थोड़ा इसपर भी सोचो तो I
वो जो समस्त जीव जगत से अतीत नहीं होता, वो मुक्त भी नहीं होता I
और ऐसा अतीत होने के लिए, तो कर्म और कर्मफलों को भी त्यागना पड़ेगा।
यही कारण है, कि …
जो मुक्ति कर्मातीत नहीं होती, वो वास्तव में कैवल्य मुक्ति भी नहीं होती।
और इसके साथ साथ …
जो कर्मातीत होती है, वो ही तो गुणातीत, भूतातीत, तन्मात्रातीत, दिशातीत या मार्गातीत, दशातीत या लोकातीत और ऐसी दशा तो कालातीत भी होती है।
ऐसी मुक्ति ही तो वो तुरीयातीत आत्मा कहलाती है…, जो वास्तव में ब्रह्म ही होता है।
ब्रह्मलीन प्रक्रिया और आत्यंतिक प्रलय …
इस ब्रह्मलीन होने की प्रक्रिया में, जब साधक की काया के भीतर का ब्रह्माण्ड, उस काया के बाहर के ब्रह्माण्ड में विलीन हो रहा होता है, तो ये स्थिति कुछ समय तक चलती भी है और ये दशा बहुत पीड़ादायक भी होती है।
ये ब्रह्मलीन होने की स्थिति इतनी प्रीडादायक होती है, की बिरले साधक ही इसमें अपनी काया को बचा सकते है। इसलिए इस प्रक्रिया में, अधिकांश साधकों का देहावसान ही हो जाता है।
इस प्रक्रिया में, वो ही बिरला साधक अपनी काया को बचा पाता है, जो अपनी भीतर की स्थिति में, ब्रह्म के समान, ब्रह्म ही होता है, जो अपने मन से ही, उस ब्रह्म के समान, पूर्ण सन्यासी होता है।
लेकिन, इन सब सिद्ध शरीरों के अपने अपने कारणों में स्वयं विलीन होने के पशचात, जो साधक के पास बचेगा, वो ही उस साधक का वास्तविक स्वरुप है, उस साधक का आत्मस्वरुप है। इसी आत्मस्वरूप को, योगीजनों नें ब्रह्म कहा है ।
यदि वो साधक, इस प्रक्रिया के समय पर, नेति नेति के वैदिक सिद्धांत में पूर्णरूपेण बसा होगा, तो ये प्रक्रिया स्वतः ही पूरी होती चली जायेगी…, अन्यथा नहीं।
अब आगे बढ़ता हूँ …
और इसके साथ साथ, यदि वो साधक, उस वाक्य में भी बसा होगा, जो मुझे गुरु भगवान वेद व्यास ने बताया था, जब ये प्रक्रिया मेरे शरीर के भीतर ही चल रही थी, और जब मैं अपने एक सूक्ष्म शरीर गमन में, उन गुरु भगवानजी के पास गया था, तो इस विलीन होने की विकट आत्यंतिक प्रलय की प्रक्रिया के समय पर, उस साधक का देहावसान नहीं होगा।
वो वाक्य जो गुरु भगवान् ने बताया था, वो ऐसा था …
देह अनात्मन् आत्मा अदेहम्
ये वाक्य, साधक के स्थूल शरीर के भीतर स्वयं प्रकट होते हुए, और स्वयं विलीन होते हुए, सभी सिद्ध शरीरों से, साधक के मन, बुद्धि, चित्त और अहम् को सुदूर रखेगा, जिससे उनके विलीन होने की प्रक्रिया में कोई ऐसी बड़ी बाधा नहीं आएगी, जिससे साधक का देहावसान ही हो जाये।
लेकिन इस वाक्य में कहे गए अदेह शब्द को, अनंत ही मानना चाहिए, नहीं तो साधक किसी सगुण निराकार देवादी लोक में ही फंस जाएगा, जब इस प्रक्रिया के समय पर, उसका कोई सिद्ध शरीर, उसके अपने मूल कारण, किसी देवादि लोक में विलीन हो रहा होगा।
और क्यूंकि इस वाक्य का वास्तविक सम्बन्ध भी संन्यास के गंतव्य, अर्थात पूर्ण संन्यास से है, इसलिए जो साधक इस वाक्य का आलम्बन अपने भाव साम्राज्य में लेगा, वो साधक भीतर से, वैसा ही सन्यासी हो जायेगा, जैसा पूर्ण सन्यासी वो ब्रह्म होता है, जो निर्गुण निराकार होता है।
और ऐसा साधक ही इस ब्रह्मलीन होने की प्रलयंकारी प्रक्रिया में, जो उस साधक के शरीर में ही चल रही होती है और जिसको आत्यंतिक प्रलय भी कहा गया है, उसमे अपना स्थूल देह सुरक्षित रख पाता है।
ब्रह्मलीन होने की स्थिति …
अब आगे बढ़ता हूँ …
जब नदी सागर में विलीन होती है, तो वो स्वयं ही अपने नदी रूप से अतीत होके ही विलीन होती है, … तुम भी ऐसे ही होगे जब तुम ब्रह्मलीन हो रहे होगे।
जैसे नदी अपने नदी स्वरुप का त्याग करके ही सागर में विलीन होती है, वैसे ही तुम भी होंगे, जब तुम अपने जीव रूप को त्यागके, शांत चित्त होके ही ब्रह्मलीन होगे।
और इसीलिये, यदि तुम ब्रह्मलीन होने के इच्छुक हो, तो अपनी इंद्रियों सहित, पंच कोषों के प्रपंचों को शांत करो।
और उन पंच कोषों के प्रपंचों को शांत करने का भी, एक ही सरल मार्ग है, कि तुम तुम्हारी अपनी भीतर की अवस्था में, “स्वयं ही स्वयं से” पृथक होके, अपने ही स्वयं-साक्षी हो जाओ।
और ऐसे हो जाओ, जैसे तुम अपने आप को ही, सूदूर से देख रहे हो।
और ऐसा होने के समय, अपने भाव में, ब्रह्म सरीके साक्षी और शांत होके, वैसे ही रहो, जैसे ब्रह्म है, जो ना ही करता है, ना ही अकरता है, और जो ना भोगता है और ना ही वो अभोगता है, जो ना ही इनमें से किसी के बीच में है, और ना ही इनसे परे ही है।
ब्रह्म को इन बतलाए हुए किसी भी स्वरुप में सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्यूंकि वो इन द्वैतवादों से परे, एकमात्र अद्वैत ही है।
वो अनंत सर्वव्याप्त ब्रह्म इन सभी द्वैतवादों के भीतर बसा हुआ भी, इनसब से परे है, क्यूंकि वो तो केवल इनका साक्षी है, और कुछ भी नहीं। और वैसे ही स्वयं साक्षी तुम भी होगे, जब तुम ब्रह्मलीन हो रहे होगे।
वो अनंत सर्वव्याप्त ब्रह्म इन सबके भीतर होता हुए भी, इन सबसे सुदूर, इन सबका एकमात्र सर्वसाक्षी ही है। इसलिए यदि तुम ब्रह्मलीन होने के इच्छुक हो, तो तुम भी ऐसे ही हो जाओ, क्यूंकि केवल ब्रह्म ही ब्रह्म का ज्ञाता होता है…, और कोई भी नहीं।
इसीलिए ब्रह्मलीम योगी जन ऐसा ही कह गए थे …
यदि ब्रह्म को जानना है, तो ब्रह्म ही हो जाओ।
ब्रह्म ही ब्रह्म का ज्ञाता होता है ।
ब्रह्म हुए बिना, ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता ।
जो साधक उसकी अपनी भावावस्था में ब्रह्म नहीं…, वो ब्रह्म का ज्ञाता भी नहीं ।
जो अनंत सर्वव्याप्त ब्रह्म है, वो सदा ही है, लेकिन तब भी उसे कुछ बिरले साधक ही जान पाते हैं। और जो साधक उसे जानते हैं, वो भी अपनी चेतना में, वो ब्रह्म होके ही, उसे जान पाते है, और वो भी उनके अपने ही आत्मस्वरूप में।
इसका कारण है, की उसको उसके वास्तविक स्वरुप में जानने को, साधक के आत्मस्वरूप के सिवा, कोई और विकल्प या मार्ग है ही नहीं।
तुम्हारे अपने आत्मस्वरुप में, तुम वो ब्रह्म ही हो क्यूंकि तुम्हारी अपनी वास्तविकता में, तुम वो हो, और वो तुम है। तुम्हारे वास्तविक स्वरुप, तुम्हारे आत्मस्वरूप के दृष्टिकोण से, तुममें और उसमें न तो कभी कोई अंतर था, और न ही कभी होगा।
यही तुम्हारा और समस्त जीव जगत का वास्तविक स्वरुप है, क्यूँकि ब्रह्म ने अपने सिवा और कुछ बनाया भी तो नहीं।
इसका कारण है, की अपनी रचना में, वो ब्रह्म अपने सीवा कुछ और बना भी तो नहीं पाया था।
रचैता ही तो उसकी अपनी रचना और उस रचना का तंत्र हुआ था। जिसको तुम रचना या रचना का तंत्र बोल रहे हो, वो ही तो रचैता है।
और यह भी तो उसी अद्वैत सिद्धांत का एक प्रमुख बिंदु है, की रचैता ही रचना और रचना का तंत्र हुआ था।
इसलिए यदि तुमको उस रचैता को जानना है, तो पहले उसकी रचना और उसकी रचना के तंत्र को अपनी काया के भीतर ही जानो। उसकी रचना और उसकी रचना के तंत्र को जाने बिना, उसे जानना असंभव ही है।
उसकी रचना में ही तो वो पाया जाता है, इसलिये तुम भी उसको “स्वयं ही स्वयं में”, पाओगे और वो भी तुम्हारे अपने आत्मस्वरूप में… और किसी भी स्वरूप में नहीं।
और क्यूंकि तुम उस ब्रह्म की रचना ही हो, और तुम्हारे भीतर ही तो उस रचना का तंत्र भी प्रकाशित हो रहा है, इसलिए तुम भी तो वो रचैता ही हो। तुम्हारे अपने जीव स्वरुप में, इस सत्य के सिवा तुम्हारा कोई और अस्तित्व है ही नहीं।
इसलिए, जो भी है इस जीव जगत के स्वरुप में, वो सब ब्रह्म ही है, ऐसा मानो…, और अपनी भीतर की स्थति में, ऐसे ही हो जाओ।
लेकिन वास्तव में, न तुम हो, न जीव है और न जगत है, क्यूंकि इन सब के स्वरुप में, बस वो अनंत ब्रह्म ही है। अपनी वास्तविकता में, यह सारा जीव जगत, वो ब्रह्म ही है, और कुछ भी नहीं।
अपनी भावनात्मक वास्तविकता में, तुम भी अपने को ऐसा ही मानो, नहीं तो ब्रह्मपथगामी ही नहीं हो पाओगे।
और ऐसा मानने से, कुछ समय के पश्चात, तुम्हारी ऐसी भावनात्मक स्थिति ही तुम्हारा ब्रह्मपथ हो जायेगी, अर्थात तुम्हारा मुक्तिमार्ग या कैवल्य मार्ग हो जाएगी।
बूंद भी बूंद, इसीलिये रही थी, क्योंकि उसकी चेतना में, वो सागर नहीं हो पाई थी। तुम भी ऐसे ही हो, इसलिये जबतक तुम अपनी चेतना में, अपने ही भावराज्य में, ब्रह्म नहीं होगे, तबतक तुम ब्रह्मपथगामी भी नहीं हो पाओगे।
और जबतक तुम ब्राहपथगामी ही नहीं होंगे, तबतक तुम उस ब्रह्म को अपने ही आत्मस्वरूप में भी नहीं पाओगे।
और ऐसी दशा में, तुम एक बूंद सरीके, अर्थात जीव सरीके ही रह जाओगे। और ऐसी स्थिति में, चाहे तुम कोइ सकारी या निराकारी देवता या उनके देवलोक ही क्यों न हो जाओ, रहोगे तो जीव या जगत स्वरुप में ही।
और ऐसी स्तिथि में, तुम उस पूर्ण सन्यासी, अमूल गन्तव्य स्वरुप निर्गुण निराकार ब्रह्म को भी अपने आत्मस्वरूप में नहीं पाओगे।
ऐसी दशा में, तुम चाहे कुछ भी पा लो, लेकिन, तुम उस अमूल गन्तव्य स्वरुप निर्गुण निराकार ब्रह्म को तो बिलकुल नहीं पा पाओगे।
और इस ब्राहपथ की एक बात याद रखो, कि …
जो गति गंतव्य तक ही नहीं होती, वो सद्गति नहीं होती।
जो सद्गति नहीं होती … वो ही तो दुर्गति कहलाती है।
इसलिए, जो गति उस गंतव्य ब्रह्म तक नहीं होती, वो ही दुर्गति कहलाती है।
और इस भाग के अंत में …
इसलिए चाहे कोई साधक किसी भी देवत्व, जीवत्व, बुद्धत्व अदि बिन्दुओं को ही क्यों न पा जाए, लेकिन जबतक वो साधक उस पूर्ण सन्यासी सन्यासी, अमूल गन्तव्य स्वरुप, निर्गुण निराकार ब्रह्म का अपने ही आत्मस्वरूप में साक्षात्कार करके, उस ब्रह्म में ही विलीन नहीं होगा, तकतक वो साधक कर्म और कर्म फलों में फंसा हुआ, दुर्गति के ही किसी न किसी स्वरुप को पाता ही चला जाएगा।
और इसी दुर्गति शब्द के कुछ सूक्ष्म और दैविक स्वरुप, देवलोकों में भी पाए जाता है, क्यूंकि देवलोक तो केवल सगुण निराकार ब्रह्म को दर्शाते है…, नाकि उस सर्वव्याप्त पूर्ण संन्यासी, सर्वसाक्षी, अद्वैत सर्वात्मा स्वरुप, निर्गुण ब्रह्म को।
मुक्तात्मा की स्थिति …
मुक्तात्मा देवत्व में नहीं होता, वो देवत्व से अतीत होता है। मुक्तात्मा जीवत्व में भी नहीं होता, वो जीवत्व से भी अतीत होता है। मुक्तात्मा जगतत्व में भी नहीं होता, वो तो जगतत्व से भी अतीत होता है।
जैसा ब्रह्म ही सार्वभौम होता है, और ब्रह्म ही सबके भीतर, सबका आत्मा होता है, और सब उस ब्रह्म के परमात्मा स्वरुप के भीतर ही बसे हुए होता है, वैसा ही मुक्तात्मा भी होता है।
इसका कारण भी वही है, जिसे वेद मनीषी कह गए थे, की, आत्मा ही तो ब्रह्म होता है। जैसा आत्मा होता है, वैसे ही तो मुक्तात्मा भी होता है।
ब्रह्म के ही सामान, वो मुक्तात्मा इस समस्त जीव जगत में और इस जीव जगत से परे भी, सामान रूप में बसा हुआ भी, इन सबसे अतीत होता है, क्यूंकि ब्रह्म के समान, वो केवल होता है, और ऐसी दशा में, वो इन सबका साक्षी ही होता है…, और कुछ भी नहीं।
अब आगे बढ़ता हूँ …
सबके अभिव्यक्ता को ब्रह्म कहते हैं और उस ब्रह्म की अभिव्यक्ति को ही प्रकृति और उसका जीव जगत कहा गया है, इसलिए इन सबके मूल में वो ब्रह्म ही है।
अभिव्यक्ति अपनी अभिव्यक्त स्थिति में, अपने अभिव्यक्ता की ओर ही अग्रसर होती है।
इसलिए, मानों या ना मानों, ये समस्त जीव जगत, उसी ब्रह्म की ओर अग्रसर है, और ऐसा ये तब से है, जबसे इसके अभिव्यक्ता ब्रह्म ने, इसे अभिव्यक्त किया था।
अभिव्यक्ति स्वरुप में भी वो एकमात्र सर्वअभिव्यक्ता ब्रह्म ही होता है, क्यूंकि वो अभिव्यक्ता अपने सीवा कुछ और अभिव्यक्त भी तो नहीं कर पाया था। इसलिए, जो अभिव्यक्ति को ही अभिव्यक्ता स्वरुप में और अभिव्यक्ता को ही अभिव्यक्ति स्वरुप में नहीं देखते, वो ब्रह्मपथगामी भी नहीं हैं क्यूंकि उनका मार्ग उस अद्वैत ब्रह्म का है ही नहीं।
मार्ग भी तो उसी अभिव्यक्ता की अभिव्यक्ति ही होते हैं, इसलिए जिस साधक के भाव साम्राज्य में ये बिंदु नहीं, वो भी ब्रह्मपथगामी नहीं ।
इसलिए …
वो ब्रह्म ही एकमात्र है, जो सबमें होता है क्यूंकि वो ब्रह्म ही सबका एकमात्र अभिव्यक्त होता है, और सब उसी एकमात्र में ही होते हैं।
और ऐसे तत्त्व को, जो सबके भीतर होता है, और जिसमें सब बसे हुए होते है, वेद मनीषियों ने आत्मा और ब्रह्म कहा है।
और इस सत्य के साक्षात्कारी साधक को ही मुक्तात्मा शब्द से सम्बोधित किया गया है। और इसके साथ साथ, जो साधक इस सत्य को जीवित अवस्था में ही साक्षात्कार कर गया, उसको ही जीवन्मुक्त कहा गया है।
जो सर्वसाक्षी मुक्तात्मा ही हो गया, उसके क्या कर्म और कर्मफल, वो तो कर्मातीत ही होता है। कर्मातीत मुक्ति भी तो कैवल्य मोक्ष को ही दर्शाती है।
और इसका मार्ग भी, तुम्हारे भीतर से ही प्रशस्त प्रशस्त होगा, जब तुम भी “स्वयं ही स्वयं में”, इस वाक्य के आत्मिक, आंतरिक सार को स्वयं ही स्वयं के होकर जाओगे।
जबतक “स्वयं ही स्वयं में” नहीं जाओगे, तबतक तुम भी यही कहते रहोगे, कि… उस ब्रह्म को कौन जान पाया है?… कोई भी तो नहीं…
उस ब्रह्म को जानने का मार्ग भी तुम्हारे आत्मास्वरूप से ही होकर जाता है।
इसलिए, जिसने भी उसे अब तक जाना है या कभी और जानेगा, वो “स्वयं ही स्वयं में” होकर ही जानेगा, क्योंकि इसके सिवा उसको जानने का कोई और मार्ग है भी तो नहीं।
लेकिन यहाँ बताए गए स्वयं शब्द की गति, तुम्हारी पिण्ड रुपी त्रिकाया से लेकर, जीव जगत तक और इससे परे तुम्हारे आत्मस्वरूप तक भी है… इसलिए इस स्वयं के शब्द ऐसा ही मानो, क्यूंकि जिसने भी उस ब्रह्म को जाना है, उसने उस ब्रह्म के पूर्ण रूप में ही जाना है।
अपूर्ण तो ब्रह्म कभी हुआ ही नहीं, इसलिए जब भी उसको जानोगे, उसके पूर्ण स्वरुप में ही जानोगे।
इसका कारण भी वही है, जो पूर्व में बताया था, कि रचैता को उसकी रचना के भीतर से ही जाना जाता है…, उसकी रचना के बाहर से नहीं। और अपने मानव रुपी जीव स्वरुप में, तुम उस ब्रह्म की एक उत्कृष्ट रचना ही तो।
इसलिए, यदि उसको जानना है, तो अपनी काया के भीतर ही जानो, क्यूंकि वो तुम्हारी काया के बाहर, तुम्हे कभी मिल ही नहीं सकता।
जब भी वो तुम्हे मिलेगा, तब वो तुम्हारे आत्मस्वरूप में ही मिलेगा, क्यूंकि जीव जगत का सार्वभौम आत्मस्वरूप भी तो वो ब्रह्म ही है।
जब भी उसे, अपने ही आत्मस्वरूप में जानोगे, तो उसके सर्वभौम स्वरूप में ही जानोगे, क्योंकि इसके सिवा, उसका और कोई स्वरूप है भी तो नहीं।
और जिस भी समय तुम उसे जानोगे, उस समय, तुम उस जैसा होकर ही उसे जानोगे, क्योंकि इसके सिवा, उसे जानने का कोई और मार्ग या विकल्प है भी तो नहीं।
इसका कारण है, कि वास्तव में तुम वो ही हो, जिसका तुमने साक्षातकार किया है, अर्थात, तुम्हारी वास्तविकता वो ही है, जिसका तुमने साक्षातकार किया है। इसलिए, ब्रह्म का साक्षात्कारी भी ब्रह्म ही होता है।
तो अब मैंने सांकेतिक रूप में ही सही, लेकिन इस योगमार्ग के, स्व:साधना के, इस मूल सत्य को बतला ही दिया है।
कुछ बिंदु खुल कर नहीं बताये जाते, क्योंकि जिव्या के देवता अग्निदेव ही होते हैं।
अपने वास्तविक स्वरूप में, अग्निदेव ही तो वो तेज रूपी, सूर्य का भी सूर्य, हिरण्य गर्भात्मक ब्रह्म की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति होते हैं, जिसके कारण वेद मनिषियों ने, अग्निदेव को भी ब्रह्म शब्द से ही सम्बोधित किया है।
तमसो मा ज्योतिर्गमय ।